Class 8th Sanskrit Chapter 1 Hindi Translation
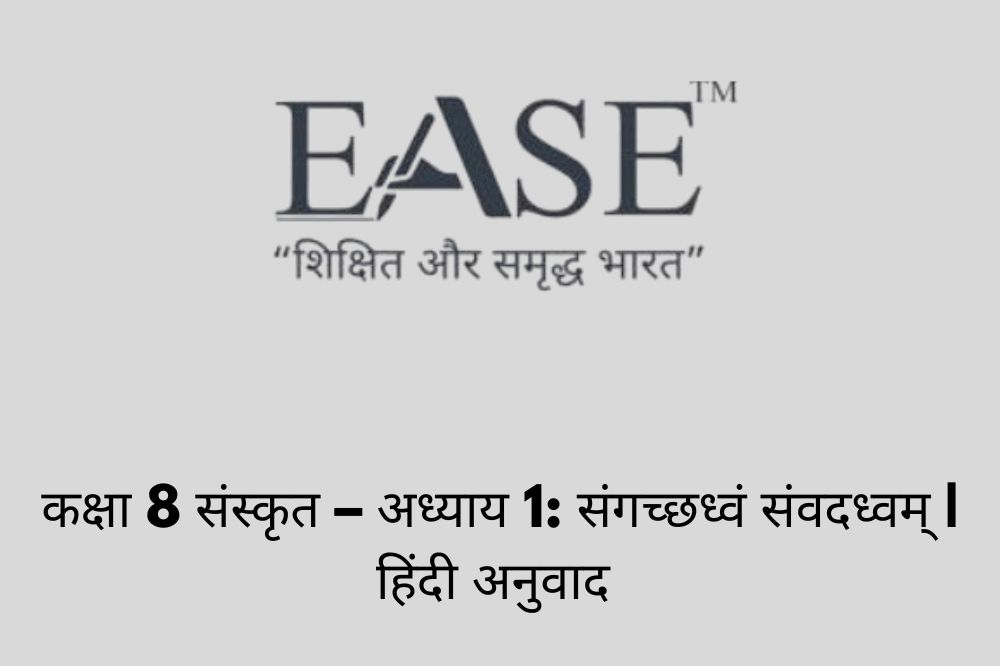
पाठ परिचय: यह पाठ ऋग्वेद के “संज्ञान सूक्त” से लिया गया है, जिसे “संघटन सूक्त” भी कहा जाता है। इसमें समाज में एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना की प्रेरणा दी गई है। Class 8th Sanskrit Chapter 1 Hindi Translation मूल मंत्र और हिंदी अनुवाद मंत्र 1: संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥ हिंदी अनुवाद: आप सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, और आपके मन एक समान हों। जैसे देवता पहले एक साथ मिलकर यज्ञ में भाग लेते थे और एकता से पूजा करते थे। मंत्र 2: समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः। समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥ हिंदी अनुवाद: आप सबका मंत्र समान हो, सभा समान हो, और मन भी समान हो। मैं आप सबके लिए एक ही मंत्र का उच्चारण करता हूँ और एक ही भावना से आहुति अर्पित करता हूँ। मंत्र 3: समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ हिंदी अनुवाद: आप सबकी इच्छाएँ समान हों, आपके हृदय एक जैसे हों। आपका मन भी एक जैसा हो, जैसे आप सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। 📚 शब्दार्थ तालिका संस्कृत शब्द हिंदी अर्थ संगच्छध्वम् मिलकर चलो संवदध्वम् मिलकर बोलो मनांसि मन भागं हिस्सा समितिः सभा मन्त्रम् विचार हविषा आहुति आकूतिः भावना हृदयानि हृदय सुसहासति सहमति से follow us Easeedu अन्वय और भावार्थ अन्वय: संगच्छध्वम् = सह गच्छत संवदध्वम् = सह वदत समानी = समान हविषा = प्रार्थनया जुहोमि = अर्पयामि भावार्थ: यह सूक्त हमें एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना का संदेश देता है। समाज में सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए, एक समान विचार रखना चाहिए और परस्पर सहयोग से ही सफलता प्राप्त होती है। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 1. सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? उत्तर: सामञ्जस्ययुक्तं और सौहार्दपूर्णं। 2. “संगच्छध्वं संवदध्वम्” इत्यस्य कः अभिप्रायः? उत्तर: सभी लोग एकता से चलें और विचार साझा करें। 3. सर्वे किं परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः? उत्तर: वैमनस्यं परित्यज्य। 4. अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? उत्तर: समाज में एकता और सहयोग की प्रेरणा। ncert solution व्याकरणिक अभ्यास – लट् से लोट् लकार लट् लकार वाक्य लोट् लकार रूप बालकाः हसन्ति बालकाः हसन्तु युवां तत्र गच्छथः युवां तत्र गच्छताम् यूयं धावथ यूयं धावत आवां लिखावः आवां लिखाव वयं पठामः वयं पठाम पाठे प्रयुक्त शब्दों का भावानुसार मेल संस्कृत शब्द भावानुसार मेल संगच्छध्वम् एक साथ चलना संवदध्वम् एक साथ बोलना मनांसि मन समितिः सभा मन्त्रम् विचार हविषा यज्ञ की आहुति आकूतिः संकल्प हृदयानि हृदय सुसहासति सहमति अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास प्रश्न: संगच्छध्वं संवदध्वम् पाठ का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: समाज में एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना को बढ़ावा देना। प्रश्न: वेदों में कितने प्रकार के उपवेद होते हैं? उत्तर: चार – आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थवेद। प्रश्न: वेदांगों के नाम बताइए। उत्तर: शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। Class 8th Sanskrit Chapter 1 Question Answer FAQs – छात्रों के लिए Q1. यह पाठ किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। Q2. ‘हविषा जुहोमि’ का अर्थ क्या है? मैं आहुति अर्पित करता हूँ। Q3. ‘समानी आकूतिः’ का भावार्थ क्या है? सबकी इच्छाएँ समान हों। Q4. यह पाठ परीक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें वैदिक संस्कृति, व्याकरण और सामाजिक संदेश तीनों का समावेश है।
Class 8th Sanskrit Chapter 1 Question Answer
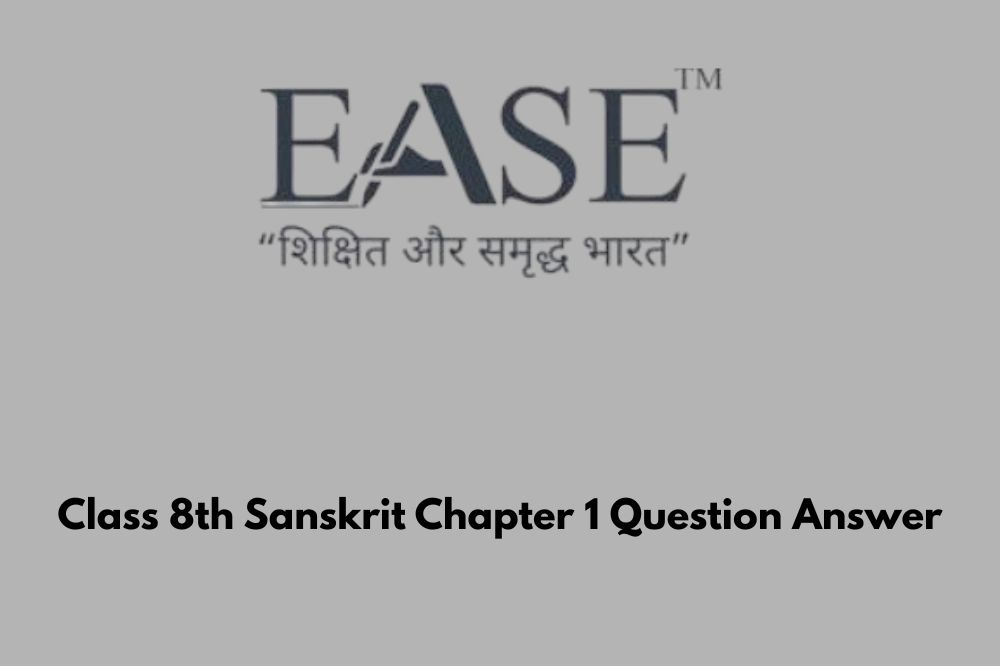
Class 8th Sanskrit Chapter 1 Question Answer | संगच्छध्वं संवदध्वम् पाठ परिचय: यह पाठ ऋग्वेद से संकलित मंत्रों पर आधारित है, जो मानव समाज को एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना की प्रेरणा देते हैं। इसमें वैदिक संस्कृति की गहराई और सामाजिक समरसता का संदेश है। अभ्यासात् जायते सिद्धिः – प्रश्न उत्तर 1. संज्ञानसूक्तं सस्वरं पठत स्मरत लिखत च। उत्तर: विद्यार्थी स्वयं सस्वर पाठ करें, स्मरण करें और लिखें। 2. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत: (क) सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? उत्तर: सर्वेषां मनः सामञ्जस्ययुक्तं सौहार्दपूर्णं च भवेत्। (ख) “सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्” इत्यस्य कः अभिप्रायः? उत्तर: इसका अभिप्राय है कि सभी लोग एकता के साथ मिलकर चलें और परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करें। (ग) सर्वे किं परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः? उत्तर: सर्वे वैमनस्यं परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः। (घ) अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? उत्तर: अस्मिन् पाठे मानव समाज को एकता, सहयोग और शांति से जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। → कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति? वयम् ईश्वरं नमामः। → वयं कं नमामः? वयम् ऐक्यभावेन जीवामः। → वयं कथं जीवामः? ईश्वरस्य प्रार्थनया शान्तिः प्राप्यते। → कस्य प्रार्थनया शान्तिः प्राप्यते? अहं समाजाय श्रमं करोमि। → अहं कस्मै श्रमं करोमि? अयं पाठः ऋग्वेदात् सङ्कलितः। → अयं पाठः कस्मात् सङ्कलितः? वेदस्य अपरं नाम श्रुतिः। → कस्य अपरं नाम श्रुतिः? मन्त्राः वेदेषु भवन्ति। → मन्त्राः कुत्र भवन्ति? पाठे प्रयुक्तान् शब्दान् भावानुसारं परस्परं योजयत शब्द मिलान करें: संस्कृत शब्द भावानुसार मेल संगच्छध्वम् एक साथ चलो संवदध्वम् एक साथ बोलो मनांसि मन भागं हिस्सा समितिः सभा मन्त्रम् विचार हविषा आहुति आकूतिः भावना हृदयानि हृदय सुसहासति सहमति से Class 9th Hindi Chapter 1 Question Answer व्याकरण अभ्यास – लट् से लोट् लकार परिवर्तन उदाहरण: बालिकाः नृत्यन्ति → बालिकाः नृत्यन्तु लट् लकार वाक्य लोट् लकार रूप बालकाः हसन्ति बालकाः हसन्तु युवां तत्र गच्छथः युवां तत्र गच्छताम् यूयं धावथ यूयं धावत आवां लिखावः आवां लिखाव वयं पठामः वयं पठाम Join us easeedu अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) Q1. संगच्छध्वं संवदध्वम् का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है – “एक साथ चलो और एक साथ बोलो।” यह एकता और सहयोग का संदेश देता है। Q2. यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? यह पाठ ऋग्वेद से संकलित है। Q3. इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना को बढ़ावा देना। Q4. मन्त्रों में प्रयुक्त ‘हविषा’ शब्द का अर्थ क्या है? ‘हविषा’ का अर्थ है – यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। Q5. इस पाठ में कौन-कौन से संस्कृत व्याकरण के विषय आते हैं? लट् लकार, लोट् लकार, शब्द मिलान, प्रश्न निर्माण आदि। Class 9th Hindi Chapter 2 Question Answer
Class 9th Hindi Chapter 3 Question Answer
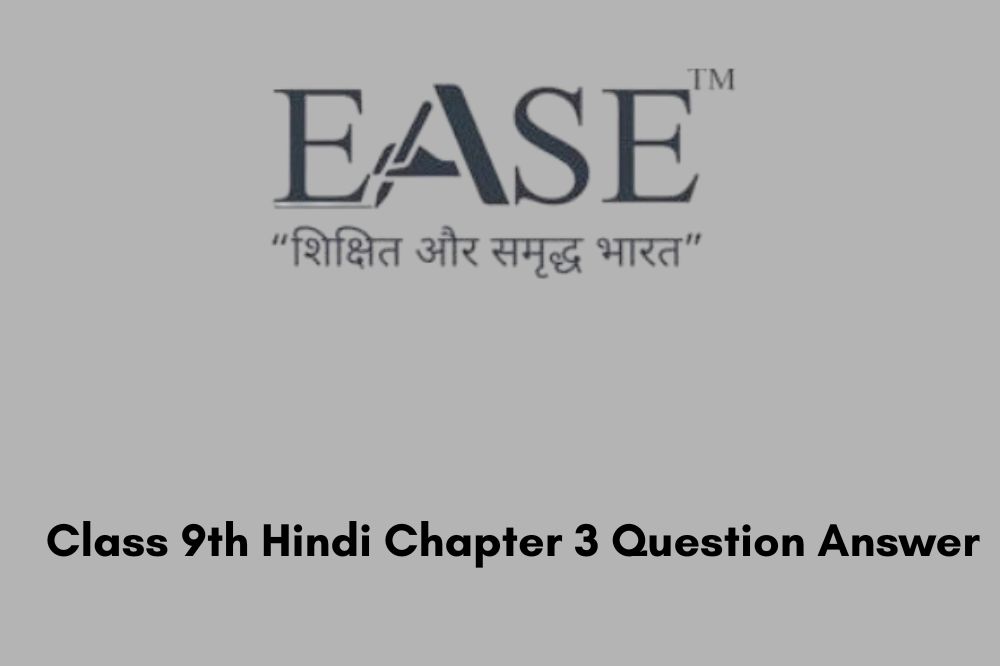
Class 9 Hindi Chapter 3 – उपभोक्तावाद की संस्कृति | NCERT Solutions with Detailed Answers Upbhoktavad ki Sanskriti by Shyama Charan Dube is a thought-provoking essay that explores the rise of consumerism in modern society. It highlights how advertisements, material desires, and blind consumption are reshaping our values, relationships, and cultural identity. Below are the NCERT questions and expert answers, rewritten for clarity, depth, and SEO performance. प्रश्न 1: लेखक के अनुसार जीवन में ‘सुख’ से क्या अभिप्राय है? उत्तर: लेखक के अनुसार, जीवन का ‘सुख’ केवल भौतिक वस्तुओं के उपभोग तक सीमित नहीं है। वास्तविक सुख में मानसिक शांति, आत्मिक संतोष, सामाजिक संबंधों की मधुरता और नैतिक संतुलन भी शामिल हैं। आज की उपभोक्तावादी सोच ने सुख को केवल वस्तुओं की उपलब्धता और विलासिता से जोड़ दिया है, जिससे व्यक्ति की आंतरिक संतुष्टि और जीवन के मूल उद्देश्य पीछे छूटते जा रहे हैं। Class 9th Hindi Chapter 2 Question Answer प्रश्न 2: आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर: वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। विज्ञापन और ब्रांडिंग के दबाव में हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं की खरीदारी करने लगे हैं। इससे न केवल आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक सरोकार भी कमजोर हो रहे हैं। व्यक्ति अब वस्तुओं के माध्यम से प्रतिष्ठा और पहचान खोजने लगा है, जिससे मानसिक तनाव, अकेलापन और आत्मकेंद्रितता बढ़ रही है। प्रश्न 3: गाँधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर: गाँधी जी का जीवन सादगी, नैतिकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक था। वे मानते थे कि भोगवादी संस्कृति व्यक्ति को स्वार्थी, असंयमी और अनैतिक बना देती है। उपभोक्तावाद के प्रभाव से समाज में वर्गभेद, दिखावा और सांस्कृतिक पतन बढ़ता है। गाँधी जी ने चेताया था कि यदि हम अपनी मूल संस्कृति और नैतिक मूल्यों से दूर हो गए, तो यह उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज की एकता और स्थायित्व के लिए गंभीर चुनौती बन जाएगी। Class 9th Hindi Chapter 1 Question Answer प्रश्न 4.1: जाने-अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर: यह कथन उपभोक्तावादी प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। व्यक्ति अब अपने विचारों, इच्छाओं और व्यवहार को बाजार और उत्पादों के अनुसार ढालने लगा है। विज्ञापन और सोशल मीडिया के प्रभाव से हम अनजाने में ही उन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। यह बदलाव हमारे चरित्र को उपभोग-केंद्रित बना रहा है, जिससे जीवन का उद्देश्य केवल वस्तुओं की प्राप्ति तक सीमित हो गया है। प्रश्न 4.2: प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। उत्तर: समाज में प्रतिष्ठा को लेकर अनेक धारणाएँ हैं, जिनमें से कई अत्यंत विचित्र और हास्यास्पद होती हैं। लोग अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए महंगी वस्तुएँ, विलासिता के साधन और अनावश्यक खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका में लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए संगीत, हरियाली और सजावट की व्यवस्था करते हैं। यह दिखाता है कि उपभोक्तावादी सोच ने मृत्यु जैसे गंभीर विषय को भी दिखावे का माध्यम बना दिया है। Surdas ke Pad Class 10 Hindi Chapter 1 प्रश्न 5: कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टी.वी. पर विज्ञापन देख कर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? उत्तर: विज्ञापन आज केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक दबाव का उपकरण बन चुके हैं। वे हमारे मन में वस्तु के प्रति आकर्षण, आवश्यकता और प्रतिष्ठा का भ्रम पैदा करते हैं। जब हम बार-बार किसी वस्तु को टीवी या सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हमारे भीतर उसे पाने की लालसा उत्पन्न होती है, चाहे वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या नहीं। यह उपभोक्तावादी मानसिकता का सीधा परिणाम है। प्रश्न 6: आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर: वस्तुओं की खरीद का आधार उनकी गुणवत्ता होना चाहिए, न कि विज्ञापन। विज्ञापन अक्सर आकर्षक दृश्य और भावनात्मक अपील के माध्यम से हमें भ्रमित करते हैं। वे वस्तु के वास्तविक गुण-दोष को छिपाकर केवल उपभोग को बढ़ावा देते हैं। गुणवत्ता पर आधारित खरीदारी न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी होती है, बल्कि यह उपभोक्ता को संतोष और स्थायित्व भी प्रदान करती है। What Is Education and Why Is It Important? प्रश्न 7: पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही “दिखावे की संस्कृति” पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: आज का समाज दिखावे की संस्कृति से ग्रस्त हो चुका है। लोग अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए महंगे मोबाइल, फैशनेबल कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएँ और विलासिता के साधन अपनाते हैं। त्योहारों, समारोहों और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी दिखावे की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह संस्कृति व्यक्ति को आत्मकेंद्रित, असंवेदनशील और भौतिकवादी बना रही है, जिससे सामाजिक संबंधों की गहराई और सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। प्रश्न 8: आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति -रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर: उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे पारंपरिक रीति-रिवाजों और त्योहारों को बाजार केंद्रित बना दिया है। पहले त्योहारों में परिवार और समाज की सहभागिता होती थी, लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धा और दिखावे का माध्यम बन गए हैं। कंपनियाँ त्योहारों को बिक्री का अवसर मानती हैं और विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। इससे त्योहारों की आत्मा, भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक महत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। What Is Education and Why Is It Important? प्रश्न 9: भाषा-अध्ययन – क्रिया-विशेषण (क) पाठ से क्रिया-विशेषण युक्त वाक्य: धीरे-धीरे समाज की सोच बदल रही है। विज्ञापन लगातार हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं। आजकल हर वस्तु की पहचान ब्रांड से होती है। उपभोक्ता हमेशा नए उत्पादों की तलाश में रहते हैं। व्यक्ति कम सोचता है, ज़्यादा खरीदता है। (ख) क्रिया-विशेषण शब्दों से वाक्य: धीरे-धीरे: धीरे-धीरे हमारी संस्कृति बदल रही है। ज़ोर से: वह ज़ोर से चिल्लाया। लगातार: वह लगातार काम कर रहा है। हमेशा: वह हमेशा समय पर आता है। आजकल: आजकल लोग
Class 9th Hindi Chapter 2 Question Answer
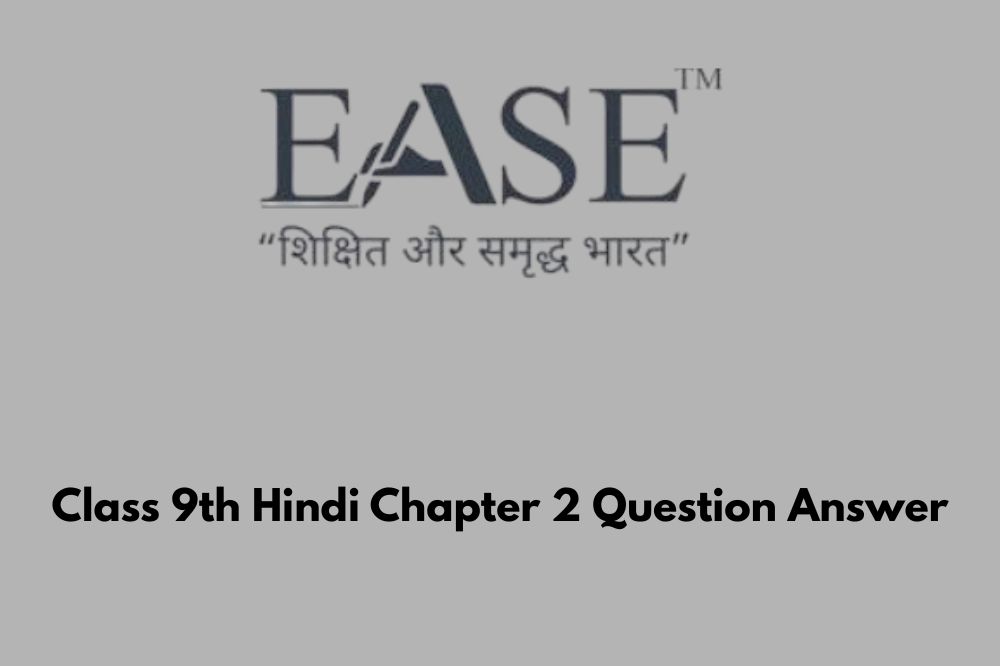
Class 9 Hindi Lhasa Ki Aur Question Answer NCERT Solutions Class 9 Hindi क्षितिज Chapter 2 Question Answer, This section includes detailed question answers from Chapter 2 – Lhasa Ki Aur, based on the Class 9 Hindi Kshitij textbook. Class 9th Hindi Chapter 1 Question Answer Each response is aligned with CBSE guidelines to support exam preparation and understanding. Class 9th Hindi Chapter 2 Question Answer | ल्हासा की ओर 1. थोंगला के पहले के आख़िरी गाँव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के वावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों ? उत्तर:- इसका मुख्य कारण था – संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक-जैसी व्यवस्थाएँ नहीं थीं। इसलिए वहाँ जान-पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान-पहचान थी। पर पाँच साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते हीं छंङ पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। 2. उस समय के तिब्बत में हथियार का क़ानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था ? उत्तर:- उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते की उनके पास पैसा है या नहीं। तथा तिब्बत में हथियार रखने से सम्बंधित कोई क़ानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बन्दूक आदि रखते थे। साथ ही, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था।लेखक 3. लंग्कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे ? उत्तर:- लेखक लंग्कोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गए थे – १. उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। २. वे रास्ता भटककर एक-डेढ़ मील ग़लत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। 4. लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परन्तु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया ? उत्तर:- लेखक ने शेकर विहार में सुमति को यजमानों के पासजाने से रोका था क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को एक सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। 5. अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाईयों का सामना करा पड़ा ? उत्तर:- लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा :- १. जगह-जगह रास्ता कठिन तो था ही साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। २. उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। ३. डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख माँगनी पड़ी ४. भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी ५. समय से न पहुँच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। ६. तेज़ धूप में चलना पड़ा था। ७. वापस आते समय लेखक को रूकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। 6. प्रस्तुत यात्रा-वृत्तान्त के आधार पर बताइए की उस समय का तिब्बती समाज कैसा था ? उत्तर:- प्रस्तुत यात्रा-वृत्तान्त के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि – १. तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति-पाँति आदि कुप्रथाएँ नहीं थी। २. सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। ३. उस समय तिब्बती की औरतें परदा नहीं करती थीं। ४. उस समय तिब्बती की जमीन जागीरदारों में बँटी थी जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। 7. ‘मैं अब पुस्तकों के भीतर था ।’नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन -सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है?y क. लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख. लेखक पुस्तकों की शैल्फ़ के भीतर चला गया। ग. लेखक के चारों ओर पुस्तकें हैं थीं। घ. पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उत्तर:- क. लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। 8. सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गाँव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर:- सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गाँव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएँ प्रकट होती हैं : जैसे – १. सुमति मिलनसार एवं हँसमुख व्यक्ति हैं। २. सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। ३. सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता हैं। ४. सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। ५. सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा। तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। ६. सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। 9. ‘हालाँकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी खयाल करना चाहिए था’। – उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार-व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। उत्तर:- सामान्यतया लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था। इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेकर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत-महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं
Class 9th Hindi Chapter 1 Question Answer
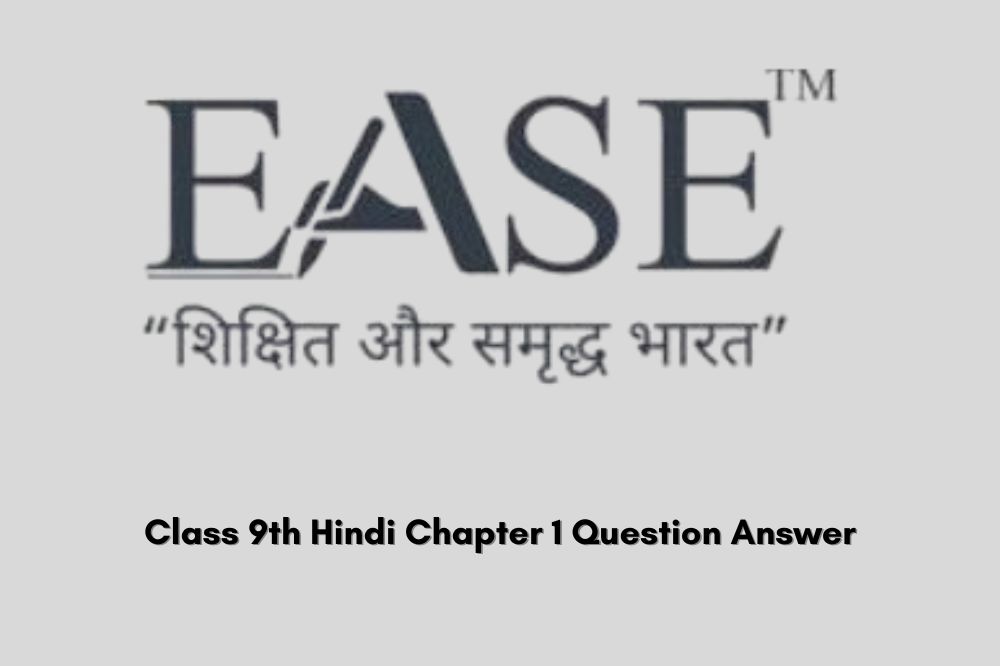
कक्षा 9 हिंदी – क्षितिज भाग 1 अध्याय 1: दो बैलों की कथा | NCERT Question & Answer Presented by EaseEdu – Grow Your CBSE School with Us | Madhav Joshi अध्याय परिचय “दो बैलों की कथा” मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक संवेदनशील और प्रेरणादायक कहानी है, जो दो बैलों – हीरा और मोती – के माध्यम से स्वतंत्रता, साहस, और मानवता के मूल्यों को उजागर करती है। यह पाठ CBSE के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भावनात्मक संबंध, शोषण के विरुद्ध संघर्ष, और नैतिक चेतना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। NCERT प्रश्नोत्तर (अभ्यास प्रश्न) प्रश्न 1: कांजीहौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर: कांजीहौस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है ताकि उनकी संख्या का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। यदि कोई पशु भाग जाए या लापता हो जाए, तो तुरंत पता लगाया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न 2: छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर: बच्ची ने अपनी माँ को खोया था और सौतेली माँ से पीड़ा झेली थी। उसने हीरा और मोती में वही पीड़ा देखी – मालिक से दूर, अत्याचार सहते हुए। भावनात्मक समानता के कारण उसके मन में बैलों के प्रति गहरा प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3: बैलों के माध्यम से कौन-कौन से नीति-विषयक मूल्य उभरते हैं? उत्तर: स्वतंत्रता का मूल्य – हर जीव का जन्मसिद्ध अधिकार। संघर्ष की आवश्यकता – स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। नारी सम्मान – स्त्री पर हिंसा को अमानवीय बताया गया है। भावनात्मक संबंध – पशु भी संवेदनशील होते हैं। Courses After 12th Commerce Courses(2026) प्रश्न 4: प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख नहीं माना, क्यों? उत्तर: गधा सहनशील, सरल और शांत स्वभाव का होता है। प्रेमचंद ने उसकी सीधापन और सहनशीलता को गुण माना, न कि मूर्खता। उन्होंने कहा – “सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा।” प्रश्न 5: हीरा और मोती की गहरी दोस्ती किन घटनाओं से स्पष्ट होती है? उत्तर: दोनों बैल एक-दूसरे का बोझ बाँटते थे। साथ उठते, बैठते, खाते और चाटते थे। मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी लौट आया – यह सच्ची मित्रता का प्रमाण है। प्रश्न 6: “औरत जात पर सींग चलाना मना है…” – इस कथन से प्रेमचंद का स्त्री दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रेमचंद ने स्त्री को सम्माननीय, पूजनीय, और सर्वोपरि माना है। उन्होंने नारी पर हिंसा को अमानवीय बताया और अपनी रचनाओं में स्त्री पात्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। प्रश्न 7: किसान जीवन में पशु और मनुष्य के संबंध कैसे हैं? उत्तर: किसान पशुओं को परिवार का हिस्सा मानते हैं। झूरी हीरा-मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता है। पशु भी अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। प्रश्न 8: “इतना तो हो ही गया…” – मोती के कथन से उसकी विशेषताएँ बताइए। उत्तर: साहसी, परोपकारी, सच्चा मित्र अत्याचार का विरोधी दयालु और संवेदनशील जानवरों की जान बचाने वाला नायक प्रश्न 9: आशय स्पष्ट कीजिए (क) “अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी…” 👉 हीरा और मोती बिना बोले एक-दूसरे के मन की बात समझते थे। यह शक्ति मनुष्य में नहीं होती। (ख) “उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती…” 👉 बच्ची की एक रोटी ने हीरा-मोती को प्रेम और अपनापन का अनुभव कराया। यह भावनात्मक तृप्ति थी। प्रश्न 10: गया ने हीरा-मोती को सूखा भूसा क्यों दिया? उत्तर: ग. वह हीरा-मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। प्रश्न 11: शोषण के खिलाफ आवाज उठाना – तर्क सहित विचार उत्तर: हीरा और मोती ने अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने भूख, मार और कैद सहकर भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। यह साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है – चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रश्न 12: क्या यह कहानी आज़ादी की ओर संकेत करती है? उत्तर: हाँ, यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। हीरा-मोती जैसे बैल संवेदनशील भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अत्याचार सहते हुए भी स्वदेश लौटने के लिए संघर्ष करते हैं। प्रश्न 13: निपात शब्दों का प्रयोग ‘ही’ निपात वाले वाक्य: एक ही विजय ने उसे गण्य बना दिया। अवश्य ही उनमें गुप्त शक्ति थी। दोनों साथ ही उठते। एक मुँह हटाता, दूसरा भी हटाता। अभी चार ही ग्रास खाए थे… ‘भी’ निपात वाले वाक्य: कुत्ता भी गरीब है… सुख-दुख में भी नहीं बदला। फिर भी बदनाम हैं। घटना अभूतपूर्व न होने पर भी… फूल की छड़ी से भी न छूता था। NIOS vs CBSE: Which Board Is Better for You (updated Guide) प्रश्न 14: वाक्य भेद और उपवाक्य वाक्य वाक्य भेद उपवाक्य भेद दीवार का गिरना था कि… संयुक्त वाक्य संज्ञा उपवाक्य सहसा एक दाढ़ियल आदमी… मिश्र वाक्य विशेषण उपवाक्य हीरा ने कहा – गया के घर… मिश्र वाक्य संज्ञा उपवाक्य मैं बेचूँगा, तो बिकेंगे। संयुक्त वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य अगर वह मुझे पकड़ता… संयुक्त वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रश्न 15: मुहावरे और प्रयोग मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग हिम्मत हारना निराश होना परीक्षा में असफल होकर उसने हिम्मत हार ली। टकटकी लगाना लगातार देखना वह दरवाज़े पर टकटकी लगाए बैठा था। जान से हाथ धोना मर जाना युद्ध में सैनिकों ने जान से हाथ धो दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना कड़ी प्रतिक्रिया सैनिकों ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दाँतों पसीना आना कठिन परिश्रम करना भारी बोझ उठाने में उसके दाँतों पसीना आ गया। अतिरिक्त प्रश्न (Extra Practice) हीरा और मोती के चरित्र में कौन-कौन से गुण हैं? झूरी का व्यवहार बैलों के प्रति कैसा था? गया के घर में बैलों की स्थिति कैसी थी? कहानी में कौन-कौन से प्रतीकात्मक संकेत हैं? प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएँ क्या हैं? Grow Your school with us : Easeedu(marketing solution for school & institute) निष्कर्ष (Conclusion) “दो बैलों की कथा” केवल पशुओं की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, संघर्ष, और संवेदना की गाथा है। CBSE छात्रों के लिए यह पाठ भावनात्मक समझ, नैतिक शिक्षा, और भाषा कौशल को विकसित करने का सशक्त माध्यम है।
Surdas ke Pad Class 10 Hindi Chapter 1 | Full Explanation & Meaning
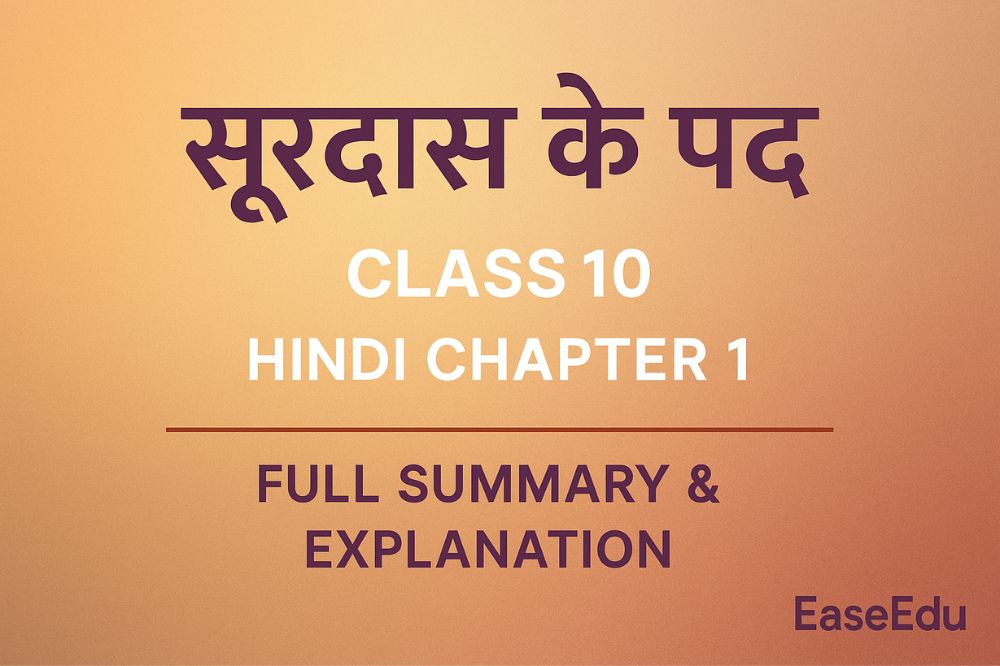
Presented by EaseEdu – Where Learning Meets Emotion | madhav Joshi Chapter Overview | Surdas ke Pad Class 10 Hindi Chapter 1 पाठ का नाम: सूरदास के पद कवि: सूरदास संग्रह: सूरसागर (भ्रमरगीत खंड) युग: भक्ति काल – सगुण भक्ति शाखा भाषा: ब्रज भाषा रस: श्रृंगार, भक्ति, विरह भाव और प्रसंग की गहराई इस अध्याय में चार पद हैं, जो गोपियों और उद्धव के बीच संवाद के रूप में रचे गए हैं। श्रीकृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव को योग और ज्ञान का संदेश देकर गोपियों को समझाने भेजा। लेकिन गोपियाँ प्रेम और भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ मानती हैं और उद्धव की बातों को व्यंग्य और तर्क से खारिज कर देती हैं। सूरदास के भ्रमरगीत के पद पाठ व्याख्या (Surdas ke Pad Class 10 Hindi Chapter 1 ) पहला पद ऊधौ , तुम हौ अति बड़भागी । अपरस रहत सनेह तगा तैं , नाहिन मन अनुरागी । पुरइनि पात रहत जल भीतर , ता रस देह न दागी । ज्यौं जल माहँ तेल की गागरि , बूँद न ताकौं लागी । प्रीति – नदी मैं पाउँ न बोरयौ , दृष्टि न रूप परागी । ‘ सूरदास ‘ अबला हम भोरी , गुर चाँटी ज्यौं पागी || पद की पंक्तियाँ और भावार्थ: “ऊधौ, तुम हौ अति बड़भागी” गोपियाँ कहती हैं—ऊधौ! तुम बहुत भाग्यशाली हो। भावार्थ: तुम श्रीकृष्ण के इतने निकट रहते हो, फिर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे। यह तुम्हारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य—हम नहीं कह सकते। “अपरस रहत सनेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी” तुम प्रेम के धागे से अछूते रहे, तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है। भावार्थ: तुम्हारा हृदय प्रेम से रहित है। तुम श्रीकृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ सके। “पुरइनि पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी” कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी गीला नहीं होता। भावार्थ: तुम भी श्रीकृष्ण के प्रेम-सागर में रहते हुए भी उसमें डूबे नहीं। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल को ग्रहण नहीं करता। “ज्यौं जल माहँ तेल की गागरि, बूँद न ताकौं लागी” जैसे तेल से सना घड़ा पानी में डूबे, फिर भी पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती। भावार्थ: तुम्हारा मन इतना कठोर है कि श्रीकृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी उसमें नहीं ठहर सकी। “प्रीति – नदी मैं पाउँ न बोरयौ, दृष्टि न रूप परागी” तुमने प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया, न ही श्रीकृष्ण के रूप में खोए। भावार्थ: तुमने न प्रेम को अपनाया, न श्रीकृष्ण के सौंदर्य में लीन हुए। तुम्हारा मन योग में उलझा रहा। “‘सूरदास’ अबला हम भोरी, गुर चाँटी ज्यौं पागी” हम भोली-भाली गोपियाँ तो श्रीकृष्ण के प्रेम में ऐसे लिप्त हैं जैसे चींटी गुड़ में चिपक जाती है। भावार्थ: हम तो पूरी तरह कृष्ण-प्रेम में डूब चुकी हैं। हमारा प्रेम गहरा, सच्चा और आत्मसमर्पण से भरा है। काव्य सौंदर्य और विशेषताएँ: तत्व विवरण भाषा ब्रज भाषा – भावपूर्ण और व्यंग्यात्मक अलंकार उपमा (कमल पत्ता, तेल घड़ा), रूपक, व्यंग्य भाव कृष्ण-वियोग, प्रेम की गहराई, योग का तिरस्कार शैली संवादात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक CBSE Class 10 SST Syllabus 2025-26 दूसरा पद मन की मन ही माँझ रही । कहिए जाइ कौन पै ऊधौ , नाहीं परत कही । अवधि अधार आस आवन की , तन मन बिथा सही । अब इन जोग सँदेसनि सुनि – सुनि , बिरहिनि बिरह दही । चाहति हुतीं गुहारि जितहिं तैं , उत तैं धार बही । ‘ सूरदास ’ अब धीर धरहिं क्यौं , मरजादा न लही । पंक्ति-दर-पंक्ति भावार्थ और व्याख्या: “मन की मन ही माँझ रही” हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। भावार्थ: गोपियाँ कहती हैं कि वे श्रीकृष्ण से जो कहना चाहती थीं, वह कभी कह नहीं सकीं। उनके प्रेम और पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया। “कहिए जाइ कौन पै ऊधौ, नाहीं परत कही” अब बताओ ऊधौ, किससे जाकर कहें? कोई समझ ही नहीं पाता। भावार्थ: गोपियाँ अपनी व्यथा किसी से साझा नहीं कर सकतीं क्योंकि कोई उनके प्रेम की गहराई को समझने योग्य नहीं है। “अवधि अधार आस आवन की, तन मन बिथा सही” कृष्ण के लौटने की आशा में समय बीतता गया, और हमने तन-मन की पीड़ा सह ली। भावार्थ: गोपियाँ श्रीकृष्ण के आने की उम्मीद में जीती रहीं, लेकिन वह आशा अधूरी रह गई। उन्होंने वियोग की पीड़ा को सहा। “अब इन जोग सँदेसनि सुनि – सुनि, बिरहिनि बिरह दही” अब बार-बार योग के संदेश सुनकर वियोगिनी गोपियाँ जल रही हैं। भावार्थ: गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव के योग-संदेश उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। वे पहले ही वियोग में जल रही थीं, अब ये बातें उन्हें और दुखी कर रही हैं। “चाहति हुतीं गुहारि जितहिं तैं, उत तैं धार बही” जहाँ वे श्रीकृष्ण से रक्षा की गुहार करना चाहती थीं, वहीं से अब आँसू की धार बह रही है। भावार्थ: गोपियाँ श्रीकृष्ण से प्रेम और सहारा चाहती थीं, लेकिन अब उनकी आँखों से केवल आँसू बहते हैं। कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। “‘सूरदास’ अब धीर धरहिं क्यौं, मरजादा न लही” अब सूरदास कहते हैं—गोपियाँ धैर्य कैसे रखें, जब उन्हें प्रेम की मर्यादा भी नहीं मिली। भावार्थ: गोपियाँ कहती हैं कि जब प्रेम में उन्हें सम्मान या उत्तर नहीं मिला, तो वे धैर्य कैसे रखें? उनका प्रेम एकतरफा और उपेक्षित रह गया। काव्य सौंदर्य और विशेषताएँ: तत्व विवरण भाषा ब्रज भाषा – भावपूर्ण और व्यंग्यात्मक अलंकार रूपक, अनुप्रास, व्यंग्य भाव कृष्ण-वियोग, प्रेम की पीड़ा, योग का तिरस्कार शैली संवादात्मक, भावनात्मक, तर्कपूर्ण तीसरा पद हमारैं हरि हारिल की लकरी । मन क्रम बचन नंद – नंदन उर , यह दृढ़ करि पकरी । जागत सोवत स्वप्न दिवस – निसि , कान्ह – कान्ह जक री । सुनत जोग लागत है ऐसौ , ज्यौं करुई ककरी । सु तौ ब्याधि हमकौं लै आए , देखी सुनी न करी । यह तौ ‘ सूर ’ तिनहिं लै सौंपौ , जिनके मन चकरी ।। पंक्ति-दर-पंक्ति भावार्थ और व्याख्या: “हमारैं हरि हारिल की लकरी” हमारे श्रीकृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी जैसे हैं। भावार्थ: गोपियाँ कहती हैं कि उनका प्रेम श्रीकृष्ण के लिए ऐसा है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है—एक बार पकड़ने के बाद उसे कभी नहीं छोड़ता। उनका
What Is Education and Why Is It Important?
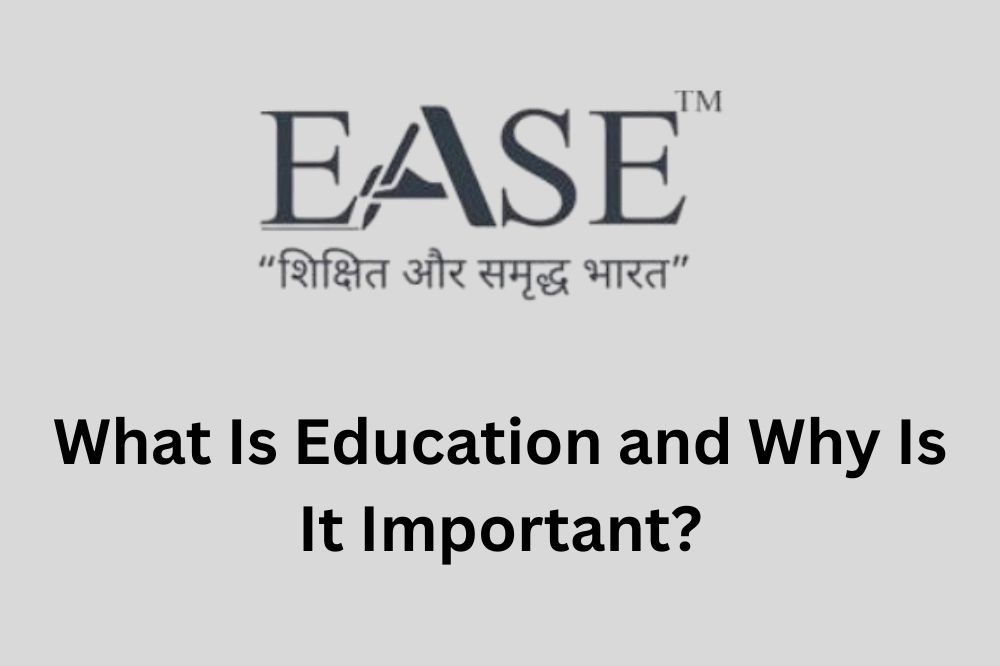
In a world driven by technology, competition, and constant change, education is no longer a luxury—it’s a necessity. It’s the foundation of personal success, national development, and global progress. Whether you’re a student preparing for board exams, a teacher shaping young minds, or a school owner building a learning ecosystem, understanding the true meaning and importance of education is essential. At EaseEdu, we believe education is not just about passing exams—it’s about unlocking human potential. This guide explores what education truly means, why it matters, and how it transforms lives at every stage. What Is Education? Education is the structured and intentional process of learning that helps individuals acquire knowledge, skills, values, and habits. It shapes how we think, communicate, solve problems, and contribute to society. Types of Education: Formal Education: School, college, and university learning with certified curricula Informal Education: Learning from life experiences, family, media, and surroundings Non-formal Education: Skill-based learning through online courses, workshops, and coaching NFAT Exam Syllabus 2025–26 Why Is Education Important? Education plays a vital role in shaping individuals and societies. Here’s how: 1. Cognitive Development and Critical Thinking Education trains the brain to think logically, solve problems, and make informed decisions. Enhances memory, focus, and reasoning Encourages curiosity and independent thinking Builds analytical and creative skills 2. Career Readiness and Economic Empowerment Education provides the qualifications and skills needed for employment and entrepreneurship. Opens doors to better job opportunities Promotes financial independence and stability Encourages innovation and business growth 3. Communication and Social Skills Education improves how we express ideas, listen, and collaborate. Builds confidence in speaking and writing Enhances teamwork and leadership Promotes respectful dialogue and empathy 4. Civic Responsibility and Social Awareness Educated citizens are more likely to engage in community service, vote responsibly, and support social justice. Promotes understanding of rights and responsibilities Encourages respect for diversity and inclusion Strengthens democratic values 5. Health Literacy and Well-being Education helps people make informed health decisions and adopt healthier lifestyles. Increases awareness of hygiene, nutrition, and safety Reduces risky behaviors and improves mental health Enhances access to healthcare resources 6. Emotional Intelligence and Personal Growth Education nurtures emotional maturity, resilience, and self-awareness. Builds empathy and compassion Supports goal-setting and motivation Helps manage stress and relationships Role of Education in Society Education is the backbone of a progressive society. It: Reduces poverty and inequality Promotes gender equality and women empowerment Encourages environmental sustainability Builds peaceful, inclusive communities Drives technological and cultural advancement Education Across Life Stages Life Stage Educational Impact Early Childhood Develops curiosity, language, and motor skills School Age Builds academic foundation and social behavior Teenage Years Shapes identity, career goals, and emotional strength Adulthood Enhances job skills, financial literacy, and decision-making Senior Years Promotes lifelong learning, wisdom sharing, and mental agility Role of Education in Skill Development FAQs – People Also Ask Q: What is the real meaning of education? Education is the lifelong process of learning that empowers individuals to grow intellectually, emotionally, and socially. Q: Why is education important for students? It helps students build knowledge, confidence, and career readiness while shaping their values and worldview. Q: How does education impact society? It reduces inequality, promotes civic responsibility, and drives economic and cultural progress. Q: Can education improve mental health? Yes. It fosters emotional intelligence, self-awareness, and access to mental health resources. Q: What are the long-term benefits of education? Better job prospects, improved quality of life, informed decision-making, and stronger communities. Conclusion: Education Is the Power Behind Progress Education is not just a tool—it’s a transformation. It empowers individuals to rise above limitations, equips societies to solve complex challenges, and fuels innovation across every sector. Whether you’re a student chasing dreams, a teacher shaping futures, or a school owner building impact, education is your strongest ally. At EaseEdu, we’re committed to making education accessible, engaging, and effective. From academic reels to SEO-rich blogs, we help institutions and learners thrive in a fast-changing world. “Education is the passport to the future. EaseEdu is your guide.” 📞 Ready to elevate your school’s educational impact? Let’s build something extraordinary—together.
